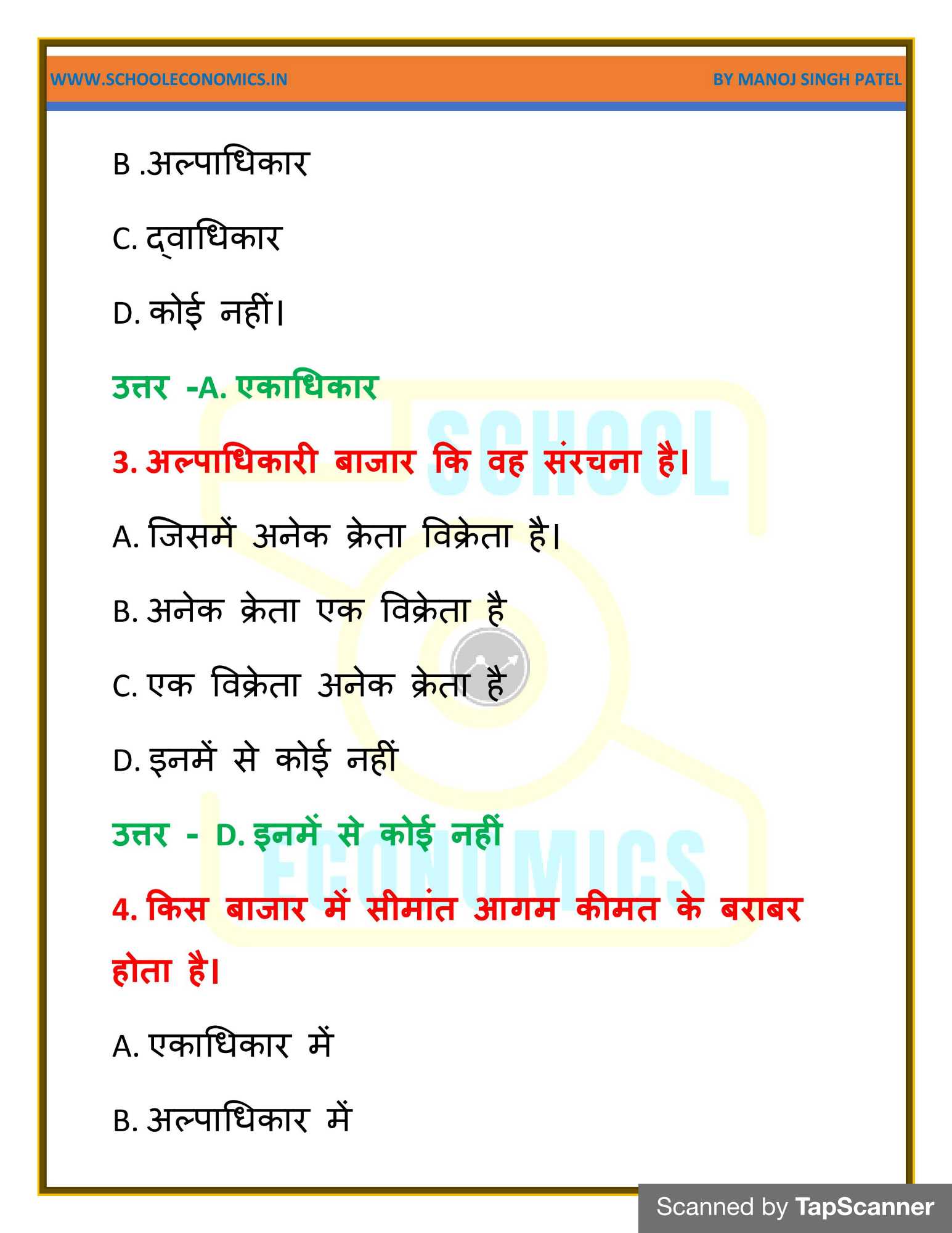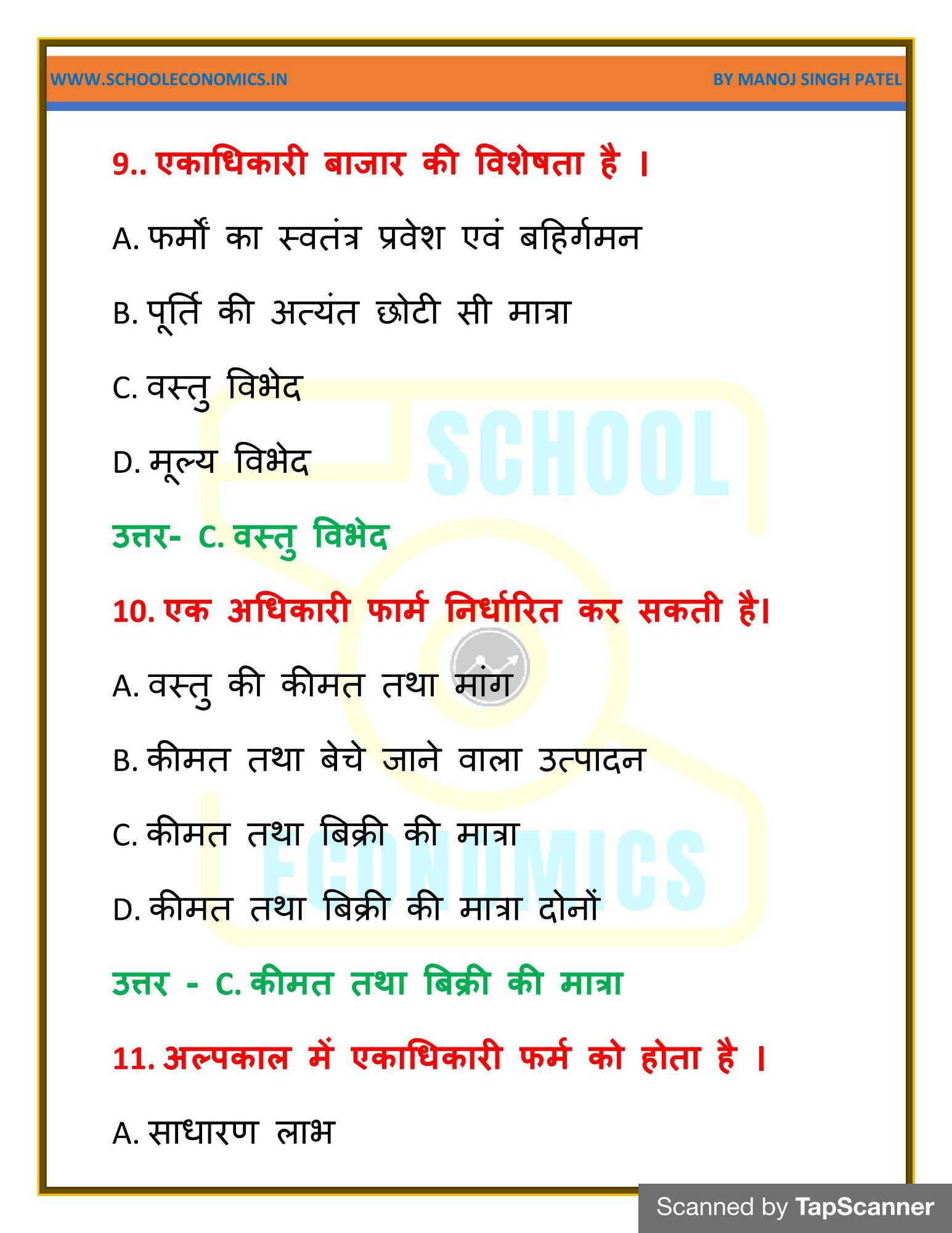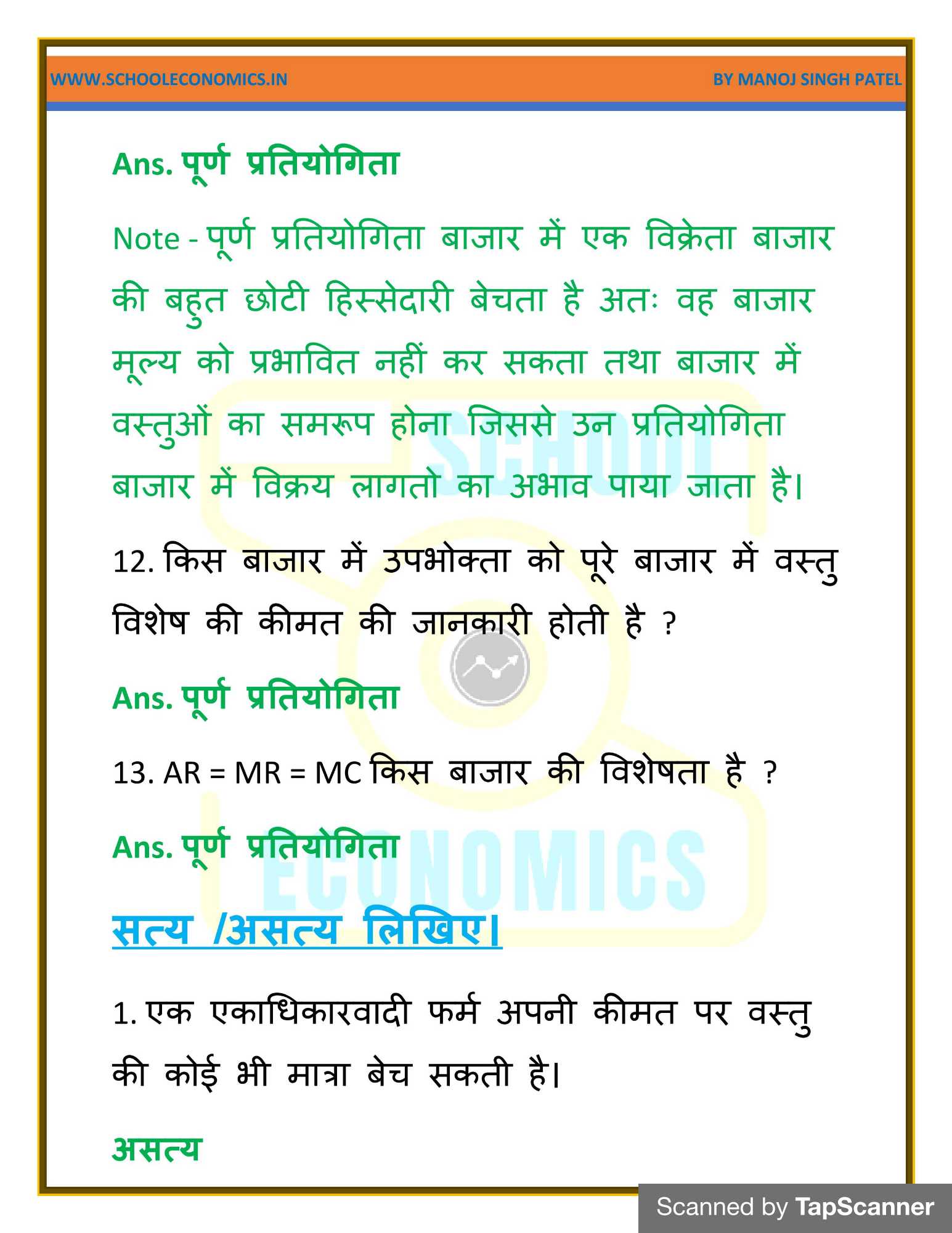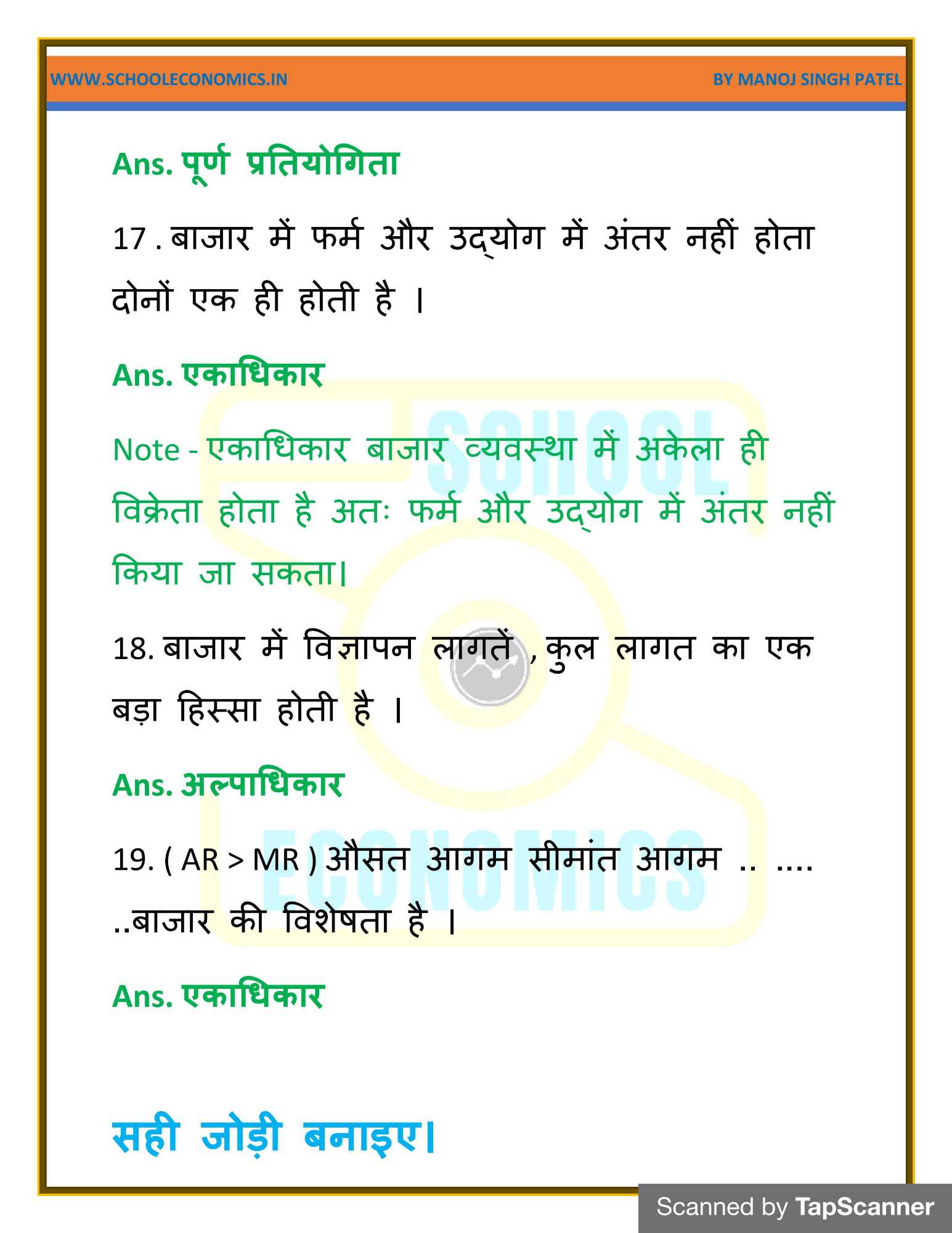व्यष्टि अर्थशास्त्र MCQ इकाई-6 प्रतिस्पर्धारहित
बाजार में बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।
बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक के परीक्षा में पूछे जाते हैं।
साथ ही साथ एक अंक के प्रश्नों में एक शब्द या एक वाक्य में
उत्तर , रिक्त स्थान , सही जोड़ियां एवं सत्य
असत्य प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे।
MCQ प्रश्न NCERT सभी Board Exam एवं प्रतियोगिता परीक्षा
में उपयोगी है।
एकाधिकार (Monopoly )
शुद्ध एकाधिकार में बाजार
में एक विक्रेता होता है एकाधिकारी माँग बाजार की माँग होती है. एकाधिकार में एट
(Zo अकेली फर्म वस्तु की एक मात्रा उत्पादक होती है जिसका को स्थानापन्न नहीं होता.
एकाधिकार शून्य प्रतियोगिता Competition) का
एक उदाहरण है. एकाधिकारी वस्तु की आड़ी माँग लोच (Cross Elastician of Demand) शून्य
या नगण्य होती है.
एकाधिकार में फर्म और उद्योग
में कोई अन्तर नहीं हो फर्म ही उद्योग है और उद्योग ही फर्म है.
विशुद्ध एकाधिकार में माँग
की लोच इकाई होती है जिससे कारण एकाधिकार के माँग वक्र के प्रत्येक बिन्दु उपभोक्ता
व्यय एक समान रहता है.
विशुद्ध एकाधिकार में औसत
आगम (AR) वक्र आयताका अतिपरवलय (Rectangular Hyperbola) होता है जिसकी माँग लोच इकाई
के बराबर होती है.
एकाधिकारी कीमत-निर्माता
(Price Maker) होता है. एकाधिकारी किसी वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति दोन को एक
साथ नियन्त्रित नहीं कर सकता. यदि वह व कीमत निर्धारित करता है तब उसे उपभोक्ता की
माँग अनुसार वस्तु पूर्ति निर्धारित करनी पड़ेगी. इसके विपरी यदि वह वस्तु की पूर्ति
निर्धारित करता है तब उस पूर्ति सम्पूर्ण बिक्री के लिए उसे उपभोक्ता द्वारा वांछित
कीमा निर्धारित करनी पड़ेगी. दोनों घटकों का निर्धारण एकाधिकार एक साथ नहीं कर सकता.
एकाधिकार में AR तथा MR का सम्बन्ध मांग लोच
निर्भर करता है.
MR = AR (e-1/e)
एकाधिकार में सीमान्त आगम
(MR) औसत आगम से कम होता है.
• एकाधिकार में नई फर्मों
का प्रवेश प्रतिबन्धित होता है. एकाधिकारी माँग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है.
एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत कितनी ऊँची रखेगा यह
माँग की लोच तथा लागत व्यवहार पर निर्भर करता है. यदि एकाधिकारी वस्तु की माँग
बेलोचदार है तब एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत ऊंची रख सकेगा और उसकी बिक्री पर कोई
विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. लोक कल्याण की दृष्टि से सरकार द्वारा रेलवे,
डाक-तार आदि पर नियन्त्रण सामाजिक एकाधिकार की श्रेणी
में आता है. एकाधिकार में अधिकतम लाभ प्राप्त
करने की दशाएँ (अथवा एकाधिकार में सन्तुलन की शर्तें) पूर्ण प्रतियोगिता की ही भाँति
होती हैं-
(i) MR = MC
(ii) सीमान्त आगम का ढाल
कम होता है सीमान्त लागत वक्र के ढाल से. एकाधिकारी कभी भी अपनी वस्तु के उत्पादन का
वह बिन्दु तय नहीं करेगा जहाँ उसके औसत आगम वक्र की लोच इकाई से कम हो. चित्र में यह
दूरी RD द्वारा प्रदर्शित है. इस दशा में MR ऋणात्मक होता है. अतः विवेकशील एकाधिकारी
सदैव यह प्रयास करता है कि वह उस बिन्दु पर उत्पादन निर्धारित करे जहाँ माँग की लोच
इकाई से अधिक है.
एकाधिकार में निश्चित पूर्ति
वक्र अनुपस्थित होता है.
एकाधिकार में एक ही पूर्ति
पर भिन्न-भिन्न कीमत उपस्थित हो सकती है. दूसरे शब्दों में माँग की विभिन्न परिस्थितियों
के कारण एक ही उत्पत्ति की मात्रा पर दो भिन्न-भिन्न कीमतें पायी जा सकती हैं. ऐसी
दशा में पूर्ति वक्र अर्थहीन (Meaningless) हो जाता है. इसी प्रकार एकाधिकार में एक
ही कीमत पर दो भिन्न-भिन्न उत्पत्ति की मात्राएं सम्भव है. ऐसी दशा में भी एकाधिकार
में पूर्ति वक्र अर्थहीन हो जाता है.
अल्पकाल में एकाधिकारी लाभ,
सामान्य लाभ तथा हानि तीनों ही स्थितियों में उत्पादन कार्य करता है. एकाधिकारी अल्पकालीन हानि की स्थिति में उस विन्दु
तक उत्पादन करना उचित समझेगा जिस बिन्दु तक उसे औसत परिवर्तनशील लागत (AVC) के बराबर
या उससे अधिक वस्तु की कीमत प्राप्त हो जाए.
दीर्घकाल में एकाधिकारी उद्योग में फर्मों का प्रवेश प्रतिबन्धित
होने के कारण एकाधिकारी सदैव लाभ अर्जित करता है, क्योंकि वह अपनी आवश्यकता और इच्छानुसार
उत्पत्ति में साधनों और अपने उत्पादन प्लाण्ट के आकार में परिवर्तन कर सकता है.
एकाधिकृत प्रतियोगिता (Monopolistic Competition)
'शुद्ध प्रतियोगिता' एवं
'शुद्ध एकाधिकार' की दोनों अवास्तविक स्थितियों के बीच वास्तविक बाजार की स्थिति को
दर्शाती हुई 1933 में दो पुस्तकें प्रकाशित हुई—
(1) The Theory of
Monopolictic Competition (E.H. Chamberlin)
(ii) The Economics of
Imperfect Competition
(Mrs. John Robinson) एकाधिकृत
प्रतियोगिता में एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है.
एकाधिकृत
प्रतियोगिता की विशेषताएं है
(i) विक्रेताओं की बड़ी
संख्या
(ii) विभिन्न फर्मों का
उत्पादन समरूप न होकर निकट स्थानापन्न
(iii) 'समूह' (Group) में
फर्मों का अप्रतिबन्धित प्रवेश एवं वहिर्गमन
(iv) विज्ञापन एवं विक्रय
लागतों (Selling Costs) की उपस्थिति
(v) गैर-मूल्य प्रतियोगिता
(Non-Price Competition)
(vi) क्रेताओं को बाजार का अपूर्ण ज्ञान
(vii) फर्मों के बीच गैर-कीमत प्रतियोगिता
(viii) प्रत्येक फर्म की अपनी कीमत नीति होती है. पूर्ण प्रतियोगिता की भाँति एकाधिकृत प्रतियोगी फर्म कीमत
प्राप्तकर्ता नहीं होती.
चैम्बरलिन के अनुसार, निकट
स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के एकत्रीकरण को 'समूह' (Group) कहा
जाता है.
● एकाधिकृत प्रतियोगिता
में वस्तुएं निकट स्थानापन्न होने के कारण माँग की आड़ी लोच ऊँची होती है. फर्म के
उत्पादन के अनेक स्थानापन्न उपलब्ध होने के कारण एकाधिकृत प्रतियोगी फर्म का माँग वक्र
अधिक लोचदार होता है.
एकाधिकृत प्रतियोगिता में
वस्तु उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता की भाँति समरूप न होकर विभेदीकृत
(Differentiated) होता है. इस बाजार में वस्तु परिवर्तन विभेदीकृत उत्पादन के कारण
उत्पन्न होता है. वस्तु परिवर्तन से अभिप्राय है वस्तु के गुण में परिवर्तन, तकनीकी
परिवर्तन एक नवीन डिजाइन, अच्छी किस्म, नई पैकिंग, शीघ्र सेवा, विनम्र विक्रेता, अच्छी
व्यापार की जगह आदि.
वस्तु परिवर्तन गैर-कीमत
प्रतियोगिता का एक अंग है. वस्तु परिवर्तन में उत्पादन लागत में परिवर्तन होता है तथा
साथ- ही-साथ माँग में भी परिवर्तन उपस्थित होता है. वस्तु परिवर्तन गुणात्मक होता है
परिमाणात्मक नहीं.
विक्रय लागतें (Selling
Costs) वे लागतें हैं जो माँग वक्र की स्थिति या आकार में परिवर्तन करने के उद्देश्य
से व्यय की जाती हैं.
विक्रय लागत = विज्ञापन पर व्यय (अखवार, ' रेडियो,
टीवी, सिनेमा द्वारा) मैनेजर, सेल्स गर्ल्स आदि का वेतन + वस्तु के प्रति आकर्षण
बढ़ाने के डीलर को दी जाने वाली रियायत व्यय + प्रदर्शनी आदि पर व्यय + उपहार
योजना आदि पर व्यय. + श +
एकाधिकृत प्रतियोगता में
विज्ञापन फर्मों के जीवन अथवा मरण का निर्धारक है. एकाधिकृत प्रतियोगी फर्म अल्पकाल
में लाभ अथवा हानि की स्थिति में रहेगी यह फर्म विशेष के आगम अथवा लग वक्रों की स्थिति
पर निर्भर करता है.
समूह का सम्पूर्ण मांग एवं
पूर्ति वक्र नहीं खींचा जा सकता। क्योंकि निकट स्थानापन्नों की माँग को एक वक्र प्रदर्शित
नहीं किया जा सकता. अतः पूर समूह का सन्तुलन • एक प्रतिनिधि फर्म के आधार पर किया जा
सकता है. समूह की फर्मों के आगम वक्र, लागत वक्र तथा उत्पादन गुण में अन्तर पाया जाता
है. प्रत्येक फर्म की कीमत निर्धारण नीति तथा मात्रा समायोजन समस्त समूह को प्रभावित करता है. समूह सन्तुलन के लिए चैम्बरलिन ने दो शौर्यपूर्ण धारणाएं (Heroic Assumptions) मानी
हैं—
(i) समता धारणा
(Uniformity Assumptions)
(ii) संगति धारणा
(Symmetry Assumptions) समता धारणा के अनुसार समूह की प्रत्येक फर्म एक समान लागत दशाओं
में कार्य करती है.
संगति धारणा के अनुसार समूह
में फर्मों की संख्या अधिक होने के कारण एक फर्म कीमत और उत्पादन परिवर्तन के लिए अन्य
प्रतियोगियों पर इतना नगण्य प्रभाव रखती है कि कोई फर्म अपनी कीमतों और उत्पादन मात्राओं
में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित नहीं होती.
• एकाधिकृत प्रतियोगिता
में फर्म दीर्घकाल की स्थिति में अनुकूलतम आकार (Optimum Size) की फर्म नहीं होती फर्म
की कुछ अनुपयुक्त क्षमता (Unutilised or Excess Capacity) शेष रहती है, क्योंकि
LAC वक्र अपने न्यूनतम बिन्दु से पहले ही AR वक्र के साथ स्पर्शी हल ( Tangency
Solution) प्राप्त कर लेता है.
दीर्घकाल में एकाधिकृत प्रतियोगी
फर्मों की संख्या बढ़ के कारण फर्मों का दीर्घकालीन माँग वक्र अधिक लोचदार जाता है.
जाने हो मार्शल, अतिरिक्त क्षमता (Excess Capacity) का विचार पीगू, विकसेल, सराफा आदि
अर्थशास्त्रियों ने भी दिया है किन्तु अतिरिक्त क्षमता सिद्धान्त की विस्तृत एवं व्याख्या
चैम्बरलिन के स्पर्शी हल (Tangency Solution) M ही मिलती है.
अल्पाधिकार एवं द्वियाधिकार (Oligopoly and Duopoly )
अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप है.
जब उद्योग में कुछ फर्में
(A few firms) एक समान वस्तुएँ (जो पूर्ण स्थानापन्न न होकर निकट स्थानापन्न होती है)
उत्पादित करती हैं तब अपूर्ण प्रतियोगिता की इस स्थिति को अल्पाधिकार कहा जाता है.
द्वियाधिकार अल्पाधिकारी
बाजार की वह विशेष परिस्थिति है जिसमें केवल दो विक्रेता होते हैं.
द्विदाधिकार के दोनों रूप
हो सकते हैं-
(i) वस्तु विभेद रहित द्वियाधिकार
(Duopoly without product differentiation)
(ii) वस्तु विभेद सहित द्वियाधिकार
(Duopoly with product differentiation)
द्वियाधिकार में उद्योग
की दोनों फर्मे आपस में गठबन्धन कर लें तो ऐसी दशा में इन्हें एकाधिकारी स्थिति प्राप्त
हो जाती हैं.
अल्पाधिकार की विशेषताएं-
(i) थोड़े विक्रेता (Few sellers )
(ii) परस्पर निर्भरता
(Inter-dependence
(iii) विज्ञापन ( Advertisement)
(iv) संघर्ष पूर्ण प्रतियोगिता (Competition)
(v) माँग वक्र की अनिश्चिता
(Indeterminateness of demand curve)
फर्मों की क्रियाओं की पारस्परिक
निर्भरता के कारण अल्पाधिकारी फर्म का माँग वक्र अनिश्चित हो जाता है.
• . कूर्नो मॉडल (1838
) की मुख्य अवधारणा यह है कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वन्द्वी विक्रेता की पूर्ति
को स्थिर मान लेता. है. कूर्नो ने खनिज स्रोतों (Mineral Springs) के उदाहरण से द्वियाधिकार
मॉडल की व्याख्या की है.