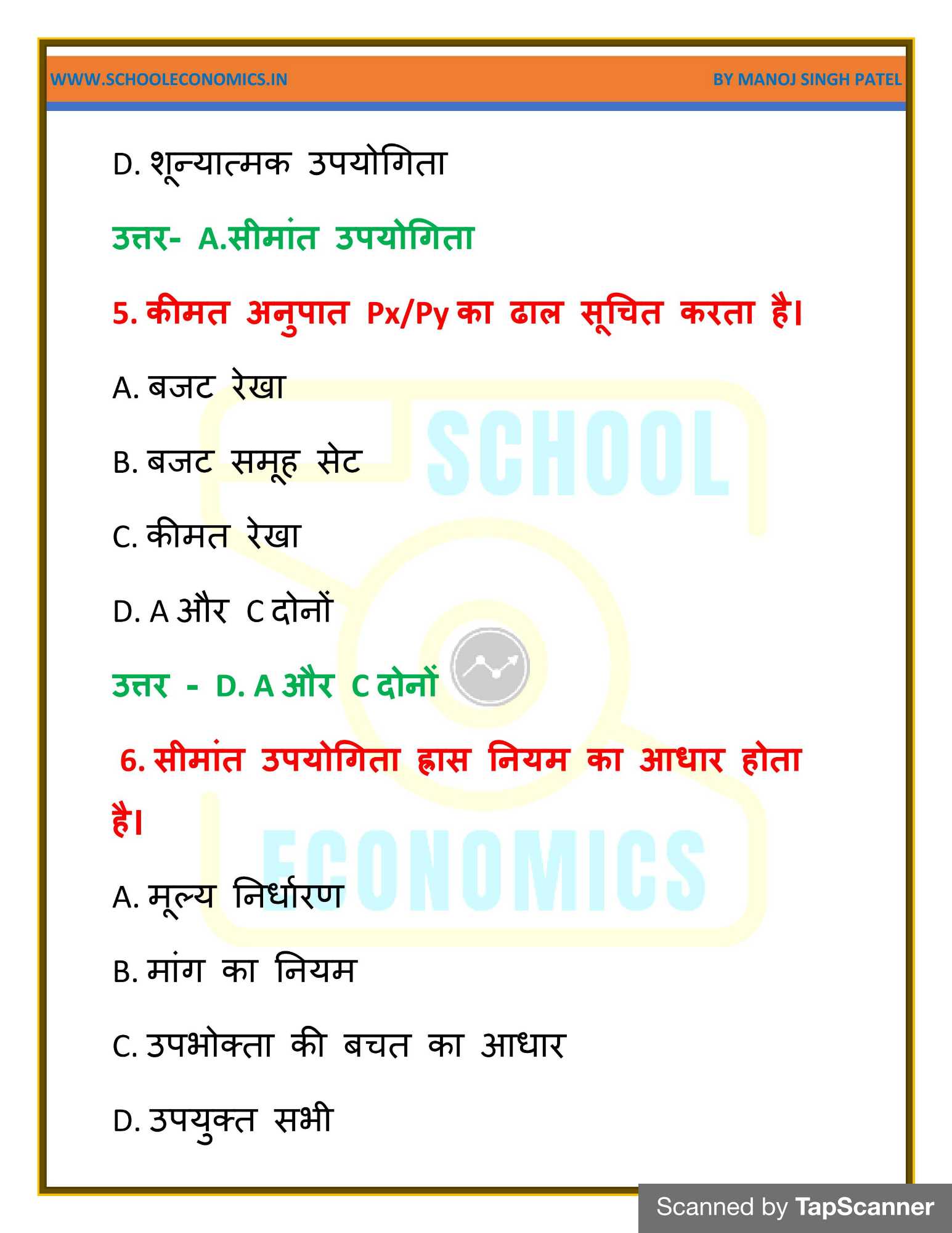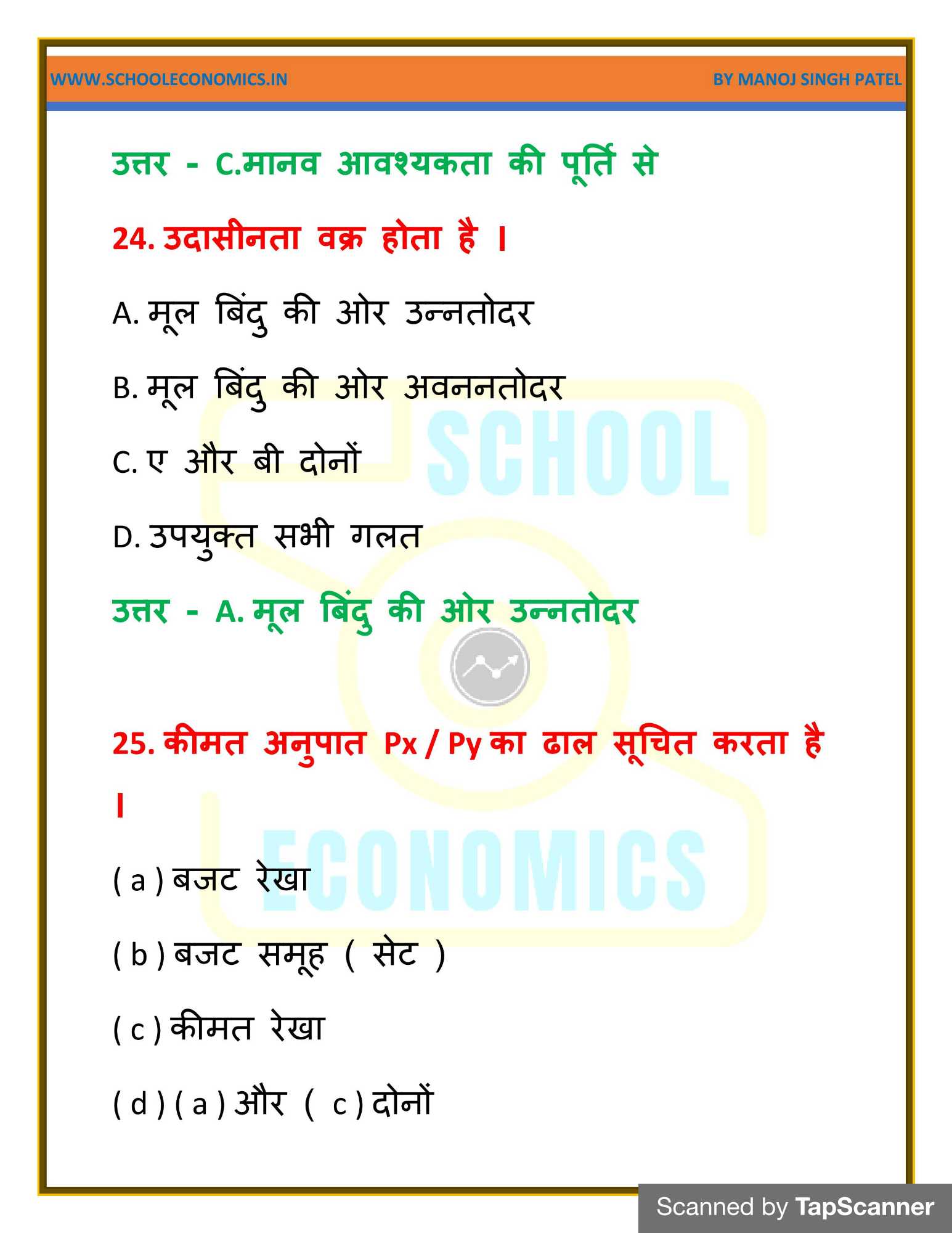व्यष्टि अर्थशास्त्र MCQ इकाई-2 उपभोक्ता व्यवहार का सिध्दांत में बहुविकल्पीय प्रश्नों का
अध्ययन करेंगे।
बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक के परीक्षा में पूछे जाते हैं।
साथ ही साथ एक अंक के प्रश्नों में एक शब्द या एक वाक्य में
उत्तर , रिक्त स्थान , सही जोड़ियां एवं सत्य
असत्य प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे।
MCQ प्रश्न NCERT सभी Board Exam एवं प्रतियोगिता परीक्षा
में उपयोगी है।
इस लिंक से फोनपे डाउनलोड करो और ₹100 कैशबैक पाये
उपभोक्ता सन्तुलन
उपभोक्ता (Consumer) अर्थशास्त्र में उपभोक्ता एक
आर्थिक एजेण्ट (Economic Agent) है, जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता
विशेष की संतुष्टि करता है।
उपभोक्ता व्यवहार
(Consumer's Behaviour)- उपभोक्ता व्यवहार का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है
जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और
सेवाओं पर किस प्रकार व्यय करे कि उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो जाये।
. उपभोक्ता संतुलन (Consumer's Equilibrium) - एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है
जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है।
दूसरे शब्दों में, जब कोई उपभोक्ता अपने व्यय करने के वर्तमान ढंग में कोई परिवर्तन
करना नहीं चाहता, तब यह उपभोक्ता संतुलन की दशा कही जाती है।
उपयोगिता (Utility) - उपयोगिता का अर्थ
है आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति अर्थात् किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की
शक्ति को उपयोगिता कहते हैं।
सीमान्त उपयोगिता (Marginal
Utility)- किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता
मिलती है, उसे सीमान्त उपयोगिता कहते हैं अर्थात् "एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग
से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमान्त उपयोगिता
(MU) कहते हैं।
• कुल उपयोगिता (Total Utility) - कुल उपयोगिता
उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमान्त उपयोगिताओं का योग होती है।
TU=E(MU)
• कुल उपयोगिता तथा सीमान्त उपयोगिता में सम्बन्ध
(Relationship between Total Utility and Marginal Utility)—
(i) जब तक वस्तु के उपभोग से मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता धनात्मक
रहती है, कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है।
iii) जब सीमान्त उपयोगिता
शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है।
(iii) जब सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता कम हो
जाती है।
घटती सीमान्त उपयोगिता नियम
(Law of Diminishing Marginal Utility) - इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की मानक
इकाइयों का लगातार उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली
सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है।
• सम सीमान्त उपयोगिता नियम (Law of
Equi-marginal Utility) - यह नियम यह बताता है कि जब सब वस्तुओं की सीमान्त
उपयोगिताओं
और उनकी कीमतों का अनुपात बराबर होता है, तब एक उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि
मिलती है।
• एक वस्तु के लिए उपभोक्ता सन्तुलन (Consumer's
Equilibrium for Single Commodity) - उपभोक्ता सन्तुलन (अधिकतम सन्तुष्टि) की स्थिति तब प्राप्त करता है,
जब प्रति रुपया सन्तुष्टि मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता (MU) के बराबर हो जाती है .
• कई वस्तुओं के लिए उपभोक्ता सन्तुलन
(Consumer's Equilibrium for Many Commodities) - उपभोक्ता सन्तुलन की स्थिति तब प्राप्त करता
है, जब प्रत्येक वस्तु की प्रति रुपया सन्तुष्टि (M1) मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता
(MU) के बराबर हो जाती है,
,• उदासीनता वक्र (Indifference Curve) - यह दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों
का बिन्दुपथ होता है जो उपभोक्ता को समान सन्तुष्टि देते हैं।।
• उदासीनता मानचित्र (Indifference Map) - एक उपभोक्ता के सन्तुष्टि के विभिन्न स्तरों
को दर्शाने वाले उदासीनता वक्रों का समूह उदासीनता मानचित्र कहलाता है।
* सीमान्त प्रतिस्थापन दर (Marginal Rate of
Substitution)- किसी वस्तु
की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को
छोड़ता है, उसे सीमान्त प्रतिस्थापन दर कहते हैं।
3. माँग वक्र बायें या नाच का 4. माँग वक्र बदल जाता है।
3. माँग वक्र पर नीचे से
ऊपर की ओर संचलन होता है। 4. माँग वक्र नहीं बदलता।
माँग (Demand ) एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी
मात्रा खरीदने को इच्छुक और योग्य होता है, उसे
कहते हैं।
माँग में पाँच तत्वों का निहित होना आवश्यक होता है-
(1) वस्तु की इच्छा।
(2) वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त
साधन।
(3) साधन व्यय करने की तत्परता।
(4) एक निश्चित कीमत।
(5) एक निश्चित समयावधि
।
● माँगी गई मात्रा (Quantity Demanded)- माँगी गई
मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो एक उपभोक्ता, एक निश्चित समय पर एक कीमत
विशेष पर खरीदने को इच्छुक और योग्य होता है।
● माँग फलन (Demand Function)- यह किसी वस्तु के लिए माँग (प्रभाव) तथा
इसके विभिन्न निर्धारक तत्वों (कारण) के बीच कार्यात्मक सम्बन्ध (या कारण तथा प्रभाव सम्बन्ध) को व्यक्त
करता है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है-
माँग तालिका
(Demand Schedule)- वह
तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के बीच के सम्बन्ध को प्रकट किया जाता है, माँग
तालिका कहलाती है।
व्यक्तिगत माँग तालिका
(Individual Demand Schedule - व्यक्तिगत माँग तालिका वह तालिका है जो किसी
निश्चित समय पर, एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को विभिन्न कीमतों पर उसकी माँग की
मात्राओं को दर्शाती है। बाजार माँग तालिका (Market Demand Schedule) - बाजार माँग
तालिका समस्त बाजार में किसी समय बिन्दु पर विभिन्न कीमतों पर
वस्तु
को माँग को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार बाजार माँग तालिका एक वस्तु के लिए कुल
उपभोक्ताओं की माँग का योग है। माँग वक (Demand Curve) माँग तालिका को जब
रेखाचित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, तब उसे माँग वक्र कहते हैं।
व्यक्तिगत माँग वक्र
(Individual Demand Curve)-व्यक्तिगत माँग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की
विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं को प्रकट
करती है।
. बाजार माँग वक्र (Market Demand Curvey - बाजार माँग वक्र तह वक्र है जो किसी वस्तु
की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा माँगी गई मात्राओं को प्रकट करता
है। बाजार माँग वक्र व्यक्तिगत माँग वक्रों का क्षैतिज योग (Horizontal Summation)
होता है।
● माँग का
नियम (Law of Demand) - माँग का नियम वस्तु की कीमत तथा इसकी माँगी गई मात्रा के बीच विपरीत सम्बन्ध
को व्यक्त करता।
हैं। इसका अर्थ है कि अन्य बातें समान रहने पर,
किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी माँग घटती तथा घटने पर माँग बढ़ती है।
माँग वक्र का ढलान ऋणात्मक
क्यों होता है? (Why does Demand Curve Slope Downwards ?) - माँग वक्र के
ऋणात्मक ढलान अथवा माँग के नियम के लागू होने के कई कारण है:
जैसे- (i) घटती सीमान्त उपयोगिता का नियम, (ii)
अन्य प्रभाव, (iii) प्रतिस्थापन प्रभाव, (iv) उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन।
● माँग के नियम के अपवाद (Exceptions to the Law
of Demand) - माँग का
नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है— (i) भविष्य में कीमत वृद्धि की सम्भावना, (ii)
प्रतिष्ठासूचक वस्तुएँ, (iii) उपभोक्ता की अज्ञानता, (iv) गिफिन का विरोधाभास ।
● आय माँग (Income Demand )
- आय माँग का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो
अन्य बातों के समान रहने की दशा में उपभोक्ता दी गई समयावधि में अपने आय के
विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता है।
● सामान्य वस्तुएँ (Normal
Goods ) - सामान्य वस्तुएँ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत
प्रभाव ऋणात्मक होता है।
• निम्नकोटि वस्तुएँ (Inferior Goods)- निम्नकोटि वस्तुएं ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका
आय प्रभाव ऋणात्मक होता है।
गिफिन वस्तुएँ (Giffin Goods ) – गिफिन वस्तु ऐसी निम्नकोटि की वस्तु है
जिसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है तथा कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। गिफिन वस्तु पर माँग का
नियम लागू नहीं होता।।
• सम्बन्धित वस्तुएँ
(Related Goods) - वस्तुएँ तब सम्बन्धित होती हैं जब (a) एक वस्तु
(X) की कीमत दूसरी वस्तु (Y) की माँग को प्रभावित करती है अथवा (b) एक
वस्तु की माँग दूसरी वस्तु की माँग में वृद्धि या कमी लाती है। सम्बन्धित वस्तुओं
को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है-
(i) स्थानापन्न वस्तुएँ तथा (ii) पूरक वस्तुएँ।
उदाहरण-कार और पेट्रोल सम्बन्धित तथा पूरक वस्तुएँ
हैं। चाय और कॉफी सम्बन्धित तथा स्थानापन्न वस्तुएँ हैं।
• स्थानापन्न वस्तुएँ (
Substitute Goods) स्थानापत्र वस्तुएँ वे सम्बन्धित वस्तुएँ हैं जो
एक-दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए,
पेप्सी कोला और कोका कोला स्थानापन्न वस्तुओं में से एक वस्तु की माँग तथा दूसरी
वस्तु की कीमत में धनात्मक सम्बन्ध होता है अर्थात् एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर
उसकी स्थानापन्न वस्तु की माँग बढ़ती है तथा कीमत कम होने पर माँग कम होती है।
• पूरक वस्तुएँ (Complementary Goods ) - पूरक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो किसी आवश्यकता
को संयुक्त रूप से सन्तुष्ट करती हैं, जैसे-पेन और स्वाही। अन्य शब्दों में, पूरक वस्तुएँ
ऐसी वस्तुएँ हैं जिनमें एक वस्तु की माँग तथा दूसरी वस्तु की कीमत में ऋणात्मक सम्बन्ध
होता है अर्थात् एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूरक वस्तु की माँग कम हो जायेगी तथा
कीमत कम होने पर पूरक वस्तु की माँग बढ़ जायेगी।
• आड़ी माँग (Cross Demand) - अन्य बातों के समान
रहने पर वस्तु X की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष सम्बन्धित वस्तु Y की माँग में जो
परिवर्तन होता है, उसे आड़ी माँग कहते हैं।
• संयुक्त माँग (Joint
Demand ) - जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की
माँग एक साथ की जाती है, तब ऐसी माँग को संयुक्त माँग कहा जाता है; जैसे- गेंद
बल्ला, स्कूटर- पेट्रोल ।
• व्युत्पन्न माँग (Derived
Demand) - जब एक वस्तु की माँग से दूसरी वस्तु की माँग स्वतः उत्पन्न हो जाती है,
तब ऐसी माँग को व्युत्पन्न माँग कहते हैं। उत्पत्ति के साधनों की माँग
व्युत्पन्न माँग होती है।
• माँग वक्र पर संचलन (Movement Along the Demand
Curve) - जब केवल किसी
वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी माँग में परिवर्तन होता है तो इसे एक ही माँग
वक्र के विभिन्न बिन्दुओं द्वारा प्रकट किया जाता है। इसे माँग वक्र पर संचलन या वस्तु
की मात्रा में परिवर्तन भी कहा जाता है। माँग वक्र पर संचलन 'माँग का विस्तार' एवं
'माँग का संकुचन' की दशाओं को बताता है। इन दोनों ही दशाओं में माँग वक्र नहीं
बदलता ।
• माँग का संकुचन (Contraction of Demand) - अन्य बातें समान रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो
माँग में होने वाली कमी को माँग का संकुचन कहते हैं। एक माँग वक्र के नीचे के
बिन्दु से ऊपर के बिन्दु की ओर संचलन माँग वक्र का खिसकाव (Shifting of the Demand
Curve) माँग वक्र के खिसकाव से अभिप्राय है कि माँग वक्र प्रारम्भिक माँग के ऊपर
या नीचे सरक जाती है। इस प्रकार का परिवर्तन तब आता है जब कीमत के अतिरिक्त दूसरे
तत्वों जैसे आय, फैशन आदि में परिवर्त
• मांग का विस्तार
(Extension of Demand)- अन्य बातें समान रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत
में कमी होने के फलस्वरूप उसकी माँग अधिक हो जाती है तो इसे माँग में
विस्तार कहा जाता है। एक माँग वक्र के ऊपर के बिन्दु से नीचे के बिन्दु की ओर
संचलन माँग का विस्तार माँग वक्र का संकुचन कहलाता है।
●माँग होने से माँग कम या अधिक हो जाती है। माँग वक्र का
खिसकाव 'माँग में वृद्धि' एवं ' माँग में कमी' की दशाओं को बताता है। इन दोनों दशा
में माँग वक्र बदल जाता है।
माँग में वृद्धि (Increase
in Demand)—- जब कीमत के अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने के कारण
वस्तु की माँग बढ़ जाते है तो इसे माँग में वृद्धि कहते हैं। यह माँग वक्र की ऊपर
की ओर खिसकाव द्वारा प्रकट होती है।
• माँग में वृद्धि के कारण (Causes of Increase
in Demand) - माँग में
वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं- (i) उपभोक्ता की आय में वृद्धि, (ii) प्रतिस्थापन
वस्तु की कीमत में वृद्धि, (ii) पूरक वस्तु की कीमत में कमी, (iv) वस्तु के लिए उपभोक्ता
की रुचि तथा प्राथमिकता में वृद्धि, (v) क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, (vi) कीमत
बढ़ने की सम्भावना, (vii) भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की सम्भावना
● माँग में
कमी (Decrease in Demand ) - जब कीमत के अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होने के कारण, वस्तु
की माँग घट जाती है तो इसे माँग में कमी कहते हैं। यह माँग वक्र की ऊपर की ओर खिसकाव
द्वारा प्रकट होती है।
माँग में कमी के कारण
(Causes of Decrease in Demand) - माँग में कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं- (1)
उपभोक्ता की आय में कमी, (ii) प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, (iii) पूरक
वस्तु की कीमत में कमी, (iv) वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता की
कमी, (v) क्रेताओं की संख्या में कमी, (vi) कीमत कम होने की सम्भावना, (vii)
भविष्य में उपभोक्ता की आय कम होने की सम्भावना ।
माँग की कीमत लोच
प्रतिशत या आनुपातिक रीति
(Percentage or Proportionate Method)—
AQ/Q
ed=- AP/P
ज्यामितीय या बिन्दु रीति (Geometric or Point Method)-
माँग वक्र पर बिन्दु का निचला भाग
माँग की लोच = माँग वक्र पर बिन्दु का ऊपर का भाग
माँग की लोच को प्रभावित
करने वाले तत्व (Factors Affecting Elasticity of Demand ) (1) वस्तु की
प्रकृति, (2) स्थानापन्न वस्तुयें, (3) वस्तु के वैकल्पिक उपयोग, (4) उपभोग स्थगन,
(5) व्यय की राशि, (6) आय-स्तर (7) कीमत-स्तर, (8) समय अवधि, (9) वस्तुओं की
पूरकता, (10) स्वभाव एवं आदत।
अधिक चपटा माँग वक्र अधिक
लोचदार होता है (Flatter the Demand Curve, Greater the Elasticity)- यदि दो माँग वक्र
एक दूसरे को काटते हैं तो कटाव बिन्दु पर जो वक्र जितना अधिक चपटा होगा, उतना ही
अधिक वह लोचशील होगा।