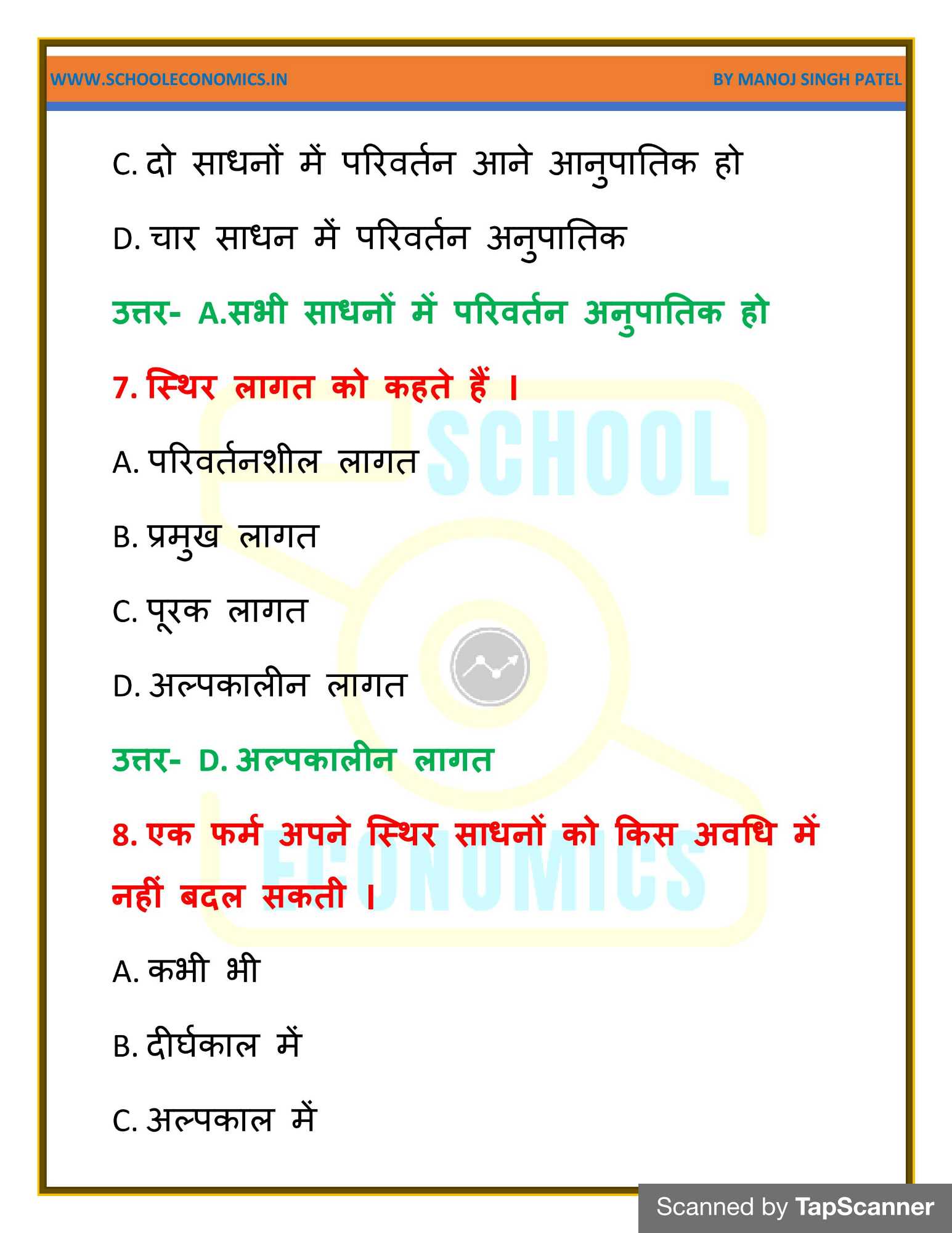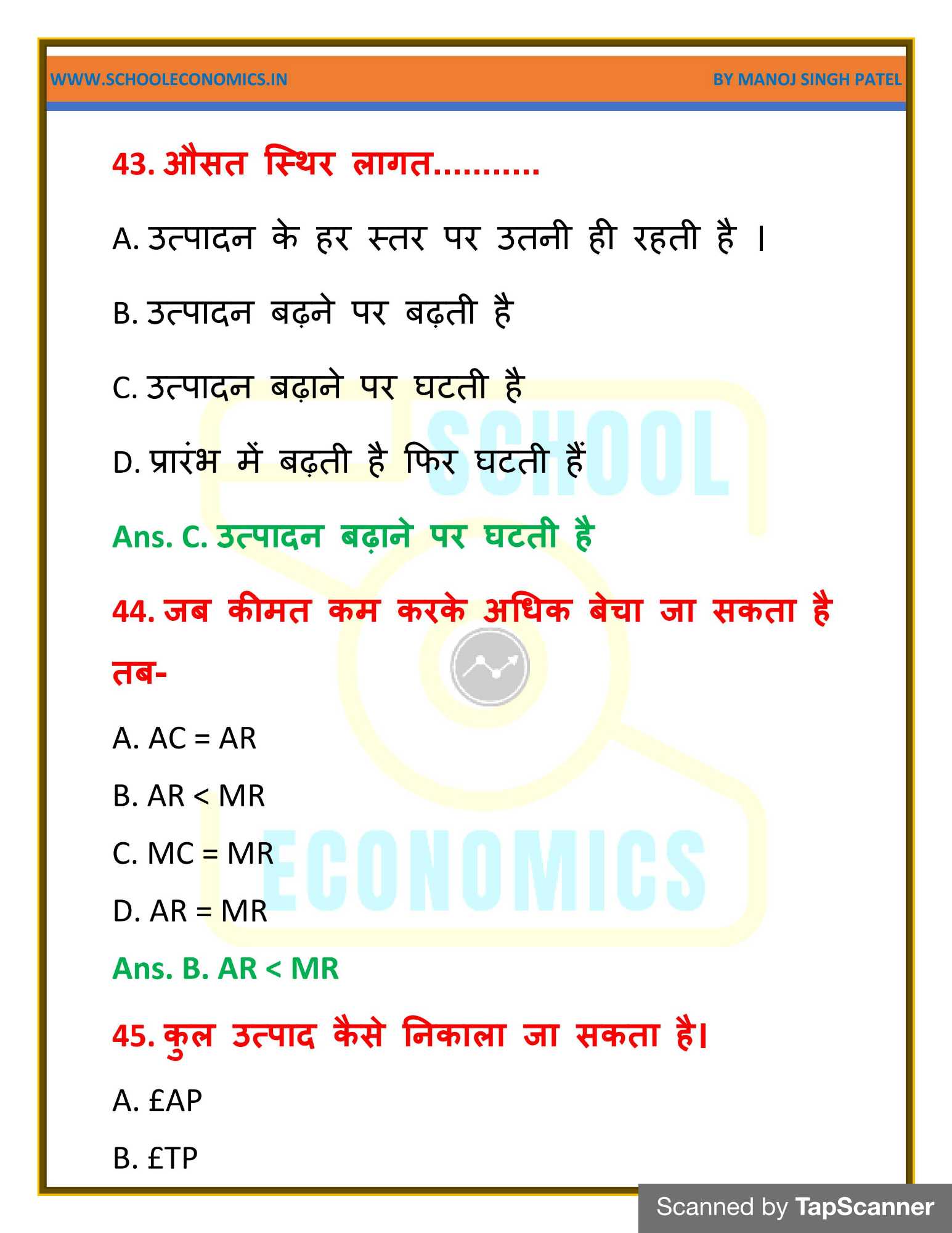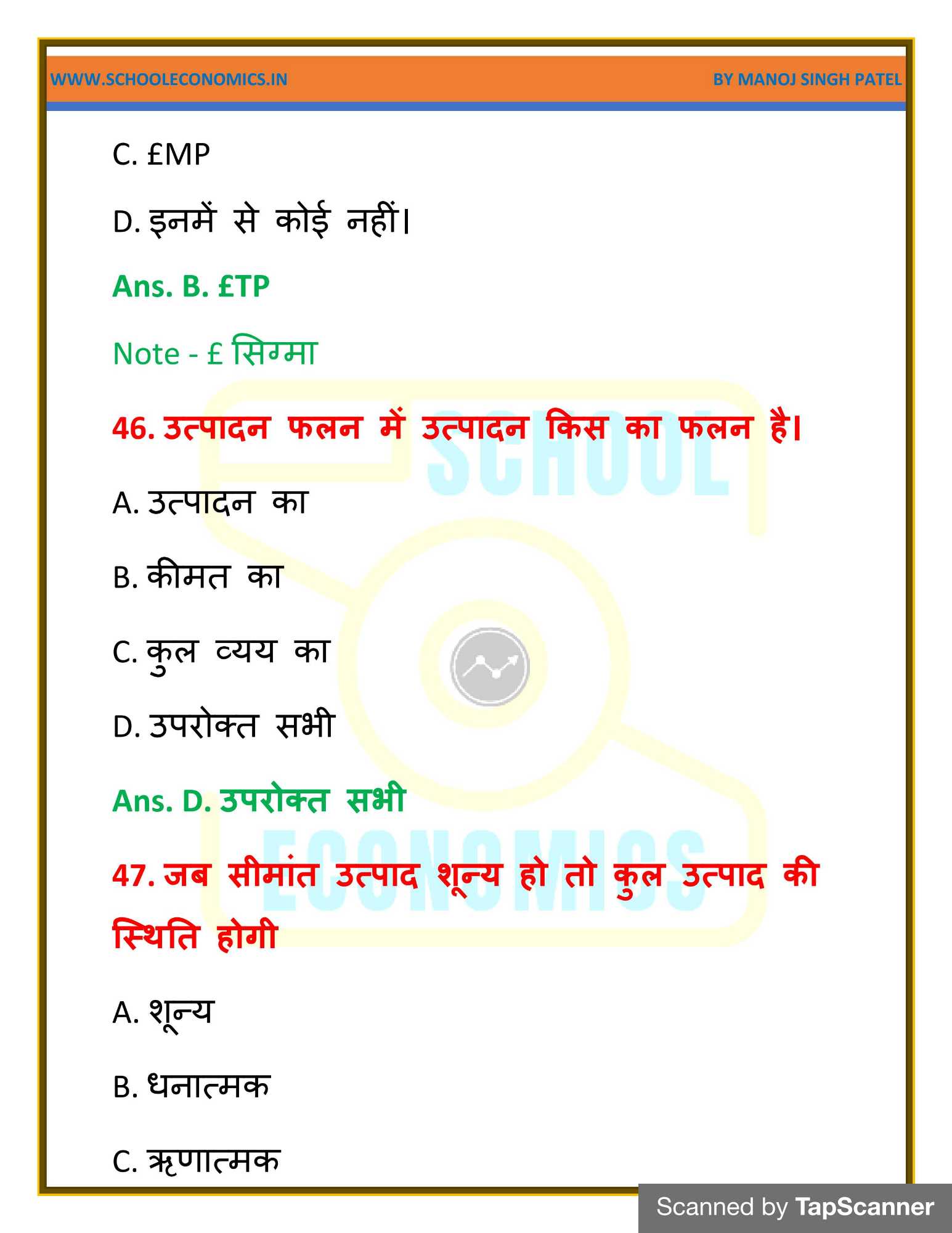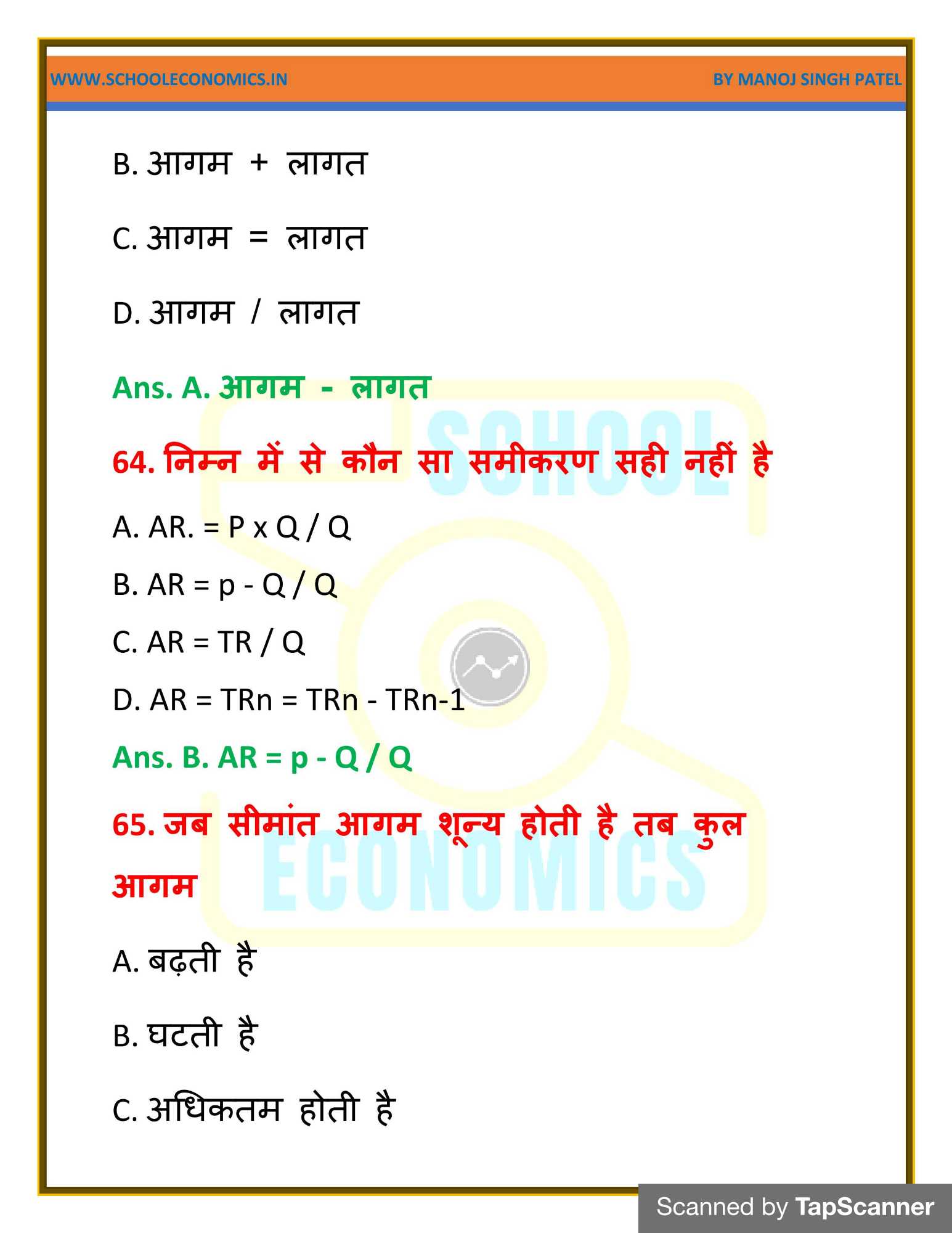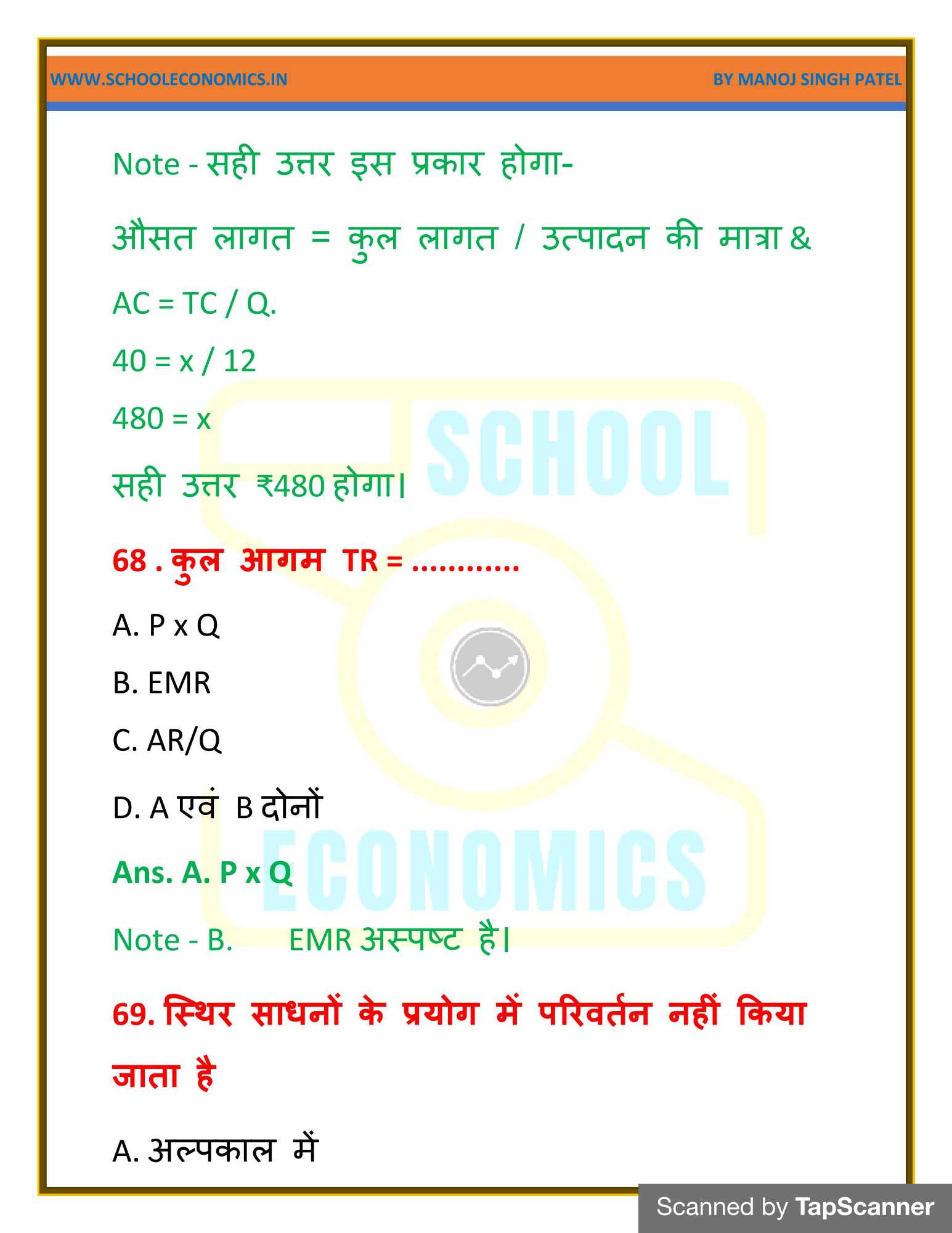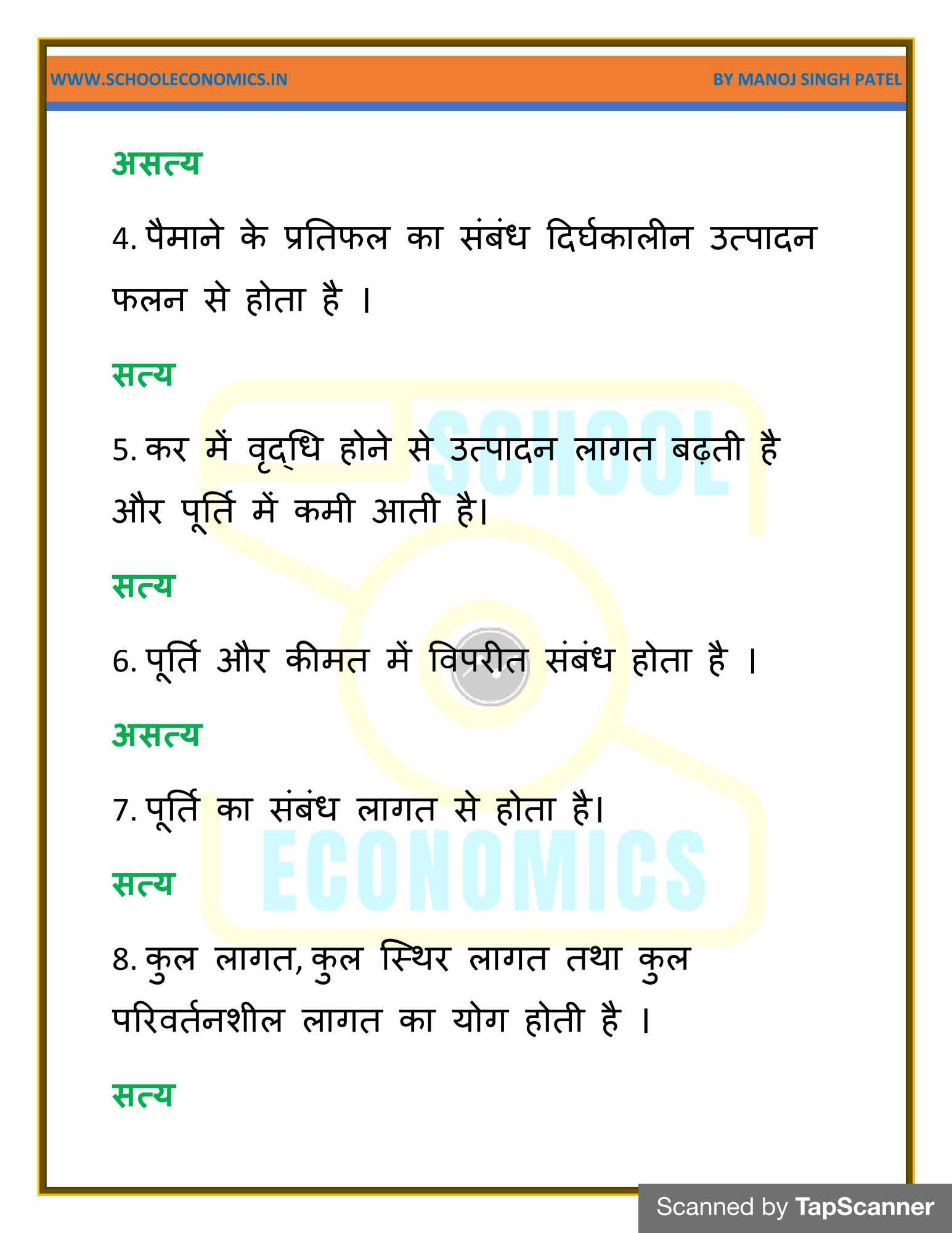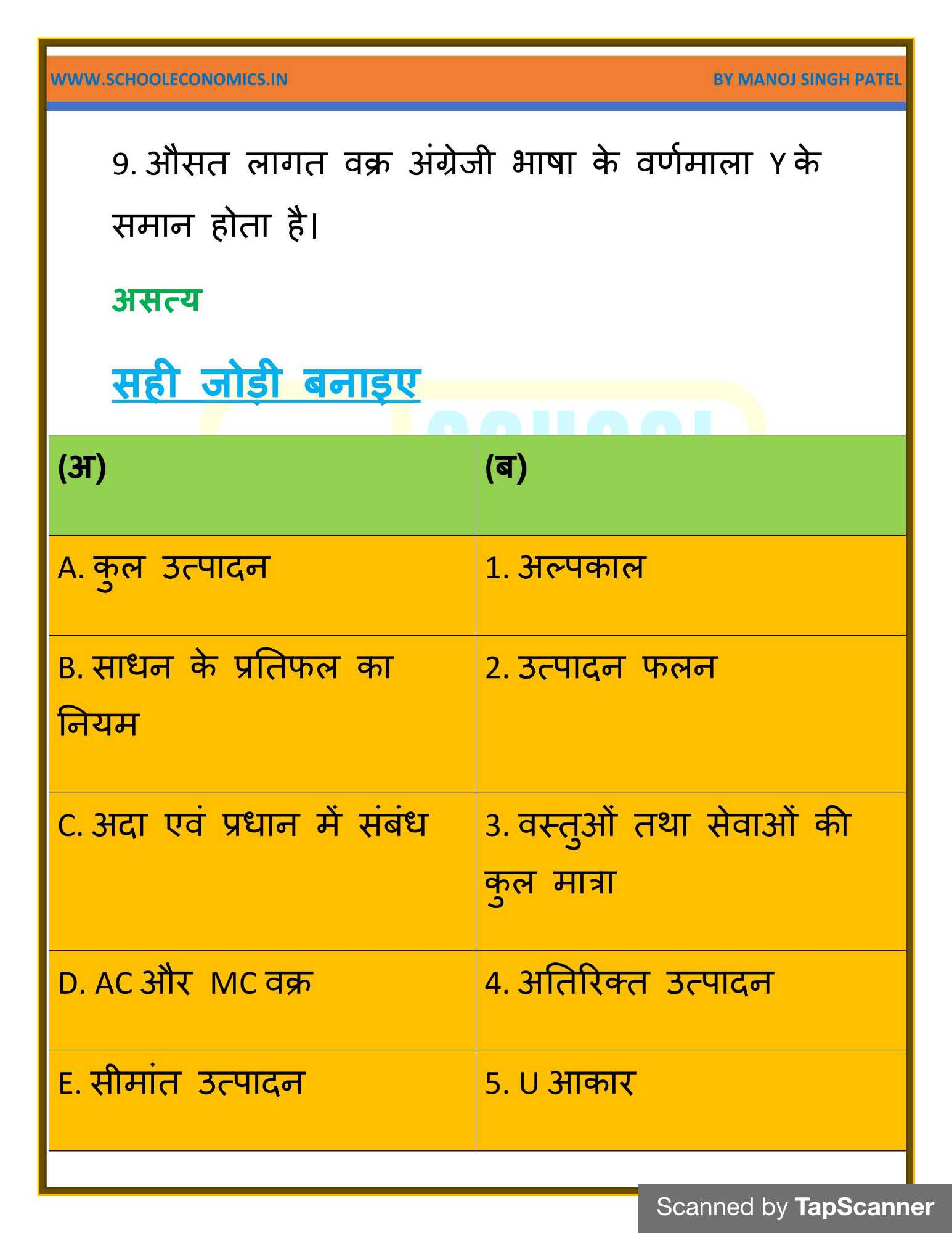व्यष्टि अर्थशास्त्र MCQ इकाई -3 उत्पादन तथा लागत
में बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।
बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक के परीक्षा में पूछे जाते हैं।
साथ ही साथ एक अंक के प्रश्नों में एक शब्द या एक वाक्य में
उत्तर , रिक्त स्थान , सही जोड़ियां एवं सत्य
असत्य प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे।
MCQ प्रश्न NCERT सभी Board Exam एवं प्रतियोगिता परीक्षा
में उपयोगी है।
उत्पादन फलन : एक साधन के
प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल
कुल उत्पादन (Total
Production)-कुल उत्पाद से अभिप्राय एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल
मात्रा से है।
औसत उत्पादन (Average
Production)- प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा को औसत उत्पादन कहा जाता है। इसे ज्ञात
करने के लिए कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की मात्रा से भाग करना पड़ता है।
AP = TP
सीमान्त उत्पादन (Marginal
Production ) - परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादन
में जो परिवर्तन होता है, उसे सीमान्त उत्पादन कहा जाता है।
उत्पादन फलन (Production
Function)- उत्पादन फलन भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच कार्यात्मक सम्बन्ध
का अध्ययन करता है। इसमें केवल भौतिक आगतों तथा उत्पादन को
ध्यान में रखा जाता है, उनके बाजार मूल्य को नहीं। Q
= f (A, B, C, D )
• उत्पादन फलन के प्रकार (Types of Production
Function)-उत्पादन फलन
निम्न दो प्रकार के होते हैं-
(i) अल्पकालीन
उत्पादन फलन या साधन के प्रतिफल (Short-run Production Function or Returns to a
Factor ) - यदि उत्पादक
उत्पादन में परिवर्तन अन्य साधनों को स्थिर रखकर उत्पादन के केवल एक ही साधन में वृद्धि
अथवा कमी के द्वारा करता है तथा इसके फलस्वरूप उत्पादन के साधनों के मिश्रण का अनुपात
बदलता है तो उत्पादन और उत्पादन के साधनों के इस सम्बन्ध को साधन का प्रतिफल या परिवर्तनशील
अनुपात का नियम कहते हैं। चूँकि इसका सम्बन्ध अल्पकाल से होता है इसलिए इसे अल्पकालीन
उत्पादन फलन कहते हैं।
(ii) दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने का प्रतिफल
(Long-run Production Function or Returns to Scale)- यदि उत्पादक सभी साधनों में एक ही अनुपात
में परिवर्तन करता है तो इस स्थिति में उत्पादन और उत्पादन के साधनों के आनुपातिक सम्बन्ध
को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। चूँकि इसका सम्बन्ध दीर्घकाल से होता है इसलिए इसे
दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन के दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं (Two
Important Types of Production Function are)-
(i) 'समान अनुपात' प्रकार का उत्पादन फलन जिसमें उत्पादन के सभी
स्तरों पर आगत-अनुपात (Input ratio) समान रहता है जो कि केवल दीर्घकाल में ही सम्भव है और
(ii)
'घटते-बढ़ते अनुपात' प्रकार का उत्पादन फलन जिसमें उत्पादन में परिवर्तन होने के
फलस्वरूप आगत-अनुपात में भी परिवर्तन होता है, केवल अल्पकाल में सम्भव है।
उत्पादन के नियम या
परिवर्तनशील अनुपात का नियम (Laws of Production or Law of Variable Proportion) घटते-बढ़ते अनुपात
के नियम के अनुसार, जब किसी एक या अधिक साधनों को स्थिर रखा जाता है तो उत्पादक के
परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में वृद्धि करने से उत्पादन पहले बढ़ते हुए अनुपात
में बढ़ता है फिर समान अनुपात में तथा इसके बाद घटते हुए अनुपात में बढ़ता है। इस
नियम के अनुसार उत्पादन की तीन अवस्थाएँ होती हैं-
पहली अवस्था (First Stage )
- सीमान्त उत्पादन अधिकतम होने के बाद घटना आरम्भ हो जाता है। औसत उत्पादन
अधिकतम हो जाता। है तथा कुल उत्पादन बढ़ता है।
दूसरी अवस्था (Second
Stage) - औसत उत्पादन घटने लगता है और कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है तथा
अधिकतम बिन्दु पर पहुँचता है, तब सीमान्त उत्पादन शून्य हो जाता है।
तीसरी अवस्था (Third Stage)
- औसत उत्पादन घटना जारी रखता है तथा कुल उत्पादन कम होने लगता है,
सीमान्त उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है।
परिवर्तनशील अनुपात का नियम
लागू होने के कारण (Causes for Operation of Law of Variable Proportion ) - (i) एक या अधिक
साधनों का स्थिर होना, (ii) साधनों की अविभाज्यता, (iii) उत्पादन साधनों का पूर्ण
स्थानापन्न होना, (iv) साधनों की सीमितता। क्या
उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित किया जा सकता है (Can the Law of
Diminishing Return be Postponed) – उत्पादन तकनीक में सुधार तथा स्थिर साधन
स्थानापन्न की खोज करके इस नियम को स्थगित किया जा सकता है।
पैमाने के प्रतिफल (Returns
to Scale)-साधनों के प्रयोग अनुपात को स्थिर रखते हुए जब सभी साधनों को समान अनुपात
में बढ़ाया जाता है, तब उत्पादन में होने वाले परिवर्तन पैमाने के
प्रतिफल से सम्बन्धित है। पैमाने के तीन प्रतिफल होते हैं- (i) पैमाने के बढ़ते
प्रतिफल, (ii) पैमाने के स्थिर प्रतिफल, (iii) पैमाने के घटते प्रतिफल । (i)
पैमाने के बढ़ते हुए या वर्द्धमान प्रतिफल (Increasing Returns to Scale) - जब
उत्पादन के सभी साधनों को K प्रतिशत बढ़ाने से उत्पादन K
प्रतिशत से अधिक बढ़ता है तो उसे पैमाने के वर्द्धमान प्रतिफल
की स्थिति कहते हैं।
(ii) पैमाने का स्थिर प्रतिफल (Constant Returns to Scale) - जब
उत्पाद के साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन अनुपात में वृद्धि होती है
तो उसे पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहते हैं। पैमाने का ह्रासमान या घटता हुआ प्रतिफल
(Decreasing Returns to Scale) जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि कर पर उत्पादन
में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे पैमाने का ह्यसमान या घटता हुआ प्रतिफल
कहते हैं।
पैमाने की आन्तरिक बचतें (Internal Economies of
Scale)- आन्तरिक बचतें
वे बचतें हैं जो किसी व्यक्तिगत फर्म के विस्तार के कारण में उपस्थित होती है।
इन बचतों का लाभ केवल उसी फर्म को मिलता है जिसमें यह बचत उत्पन्न होती है।
• पैमाने की आन्तरिक बचतों
के प्रकार (Types of Internal Economies of Scale)—
(i) श्रम
विभाजन एवं विशिष्टीकरण की बचतें।
(ii) तकनीकी बचतें (प्लाण्ट का अनुकूलतम प्रयोग)।
(ii) प्रबन्धकीय बचतें।
(iv) विपणन की बचतें।
(v) वित्तीय बचते
पैमाने की बाहरी बचतें
(External Economies of Scale)-बाहरी बचतें वे बचते हैं जो उद्योग के विस्तार के
कारण उपस्थित होती हैं त जिनका लाभ एक या दो फर्मों तक केन्द्रित न होकर उद्योग की
सभी फर्मों के लिए समान रूप से होता है।
• पैमाने की बाहरी बचतों के प्रकार (Types of
External Economies of Scale)-
(vi) [जोखिम सम्बन्धी बचतें।
(i) कुशल श्रम की उपलब्धता । (ii) परिवहन एवं संचार साधनों का विस्तार।
(iii) वित्तीय संस्थाओं का विकास। (iv) कच्चे माल की आपूर्ति ।
(v) प्रशिक्षण द्वारा श्रमिक कार्यक्षमता में सुधार।
● वास्तविक लागत (Real Cost)-- वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयत्नों
तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में पढ़ते हैं। वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जाता
है क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट एवं त्याग का सामना करना पड़ता है।
अवसर लागत (Opportunity Cost) - किसी वस्तु X की अवसर लागत दूसरी वस्तु Y की वह कीमत
है जिसका वस्तु X का उत्पादन कर के लिए त्याग करना पड़ता है।
:- स्पष्ट
लागत (Explicit Coat)-
स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान है जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं
तथा वस्तुओं के लिए दिये जाते है।
अस्पष्ट अग्रवा
सन्निहित लागत (Implicit Cost)- अस्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जो किसी फर्म के अपने साधनों के प्रयोग
के फलस्वरूप उत्पादन लागतें उत्पन्न होती है। इनका भुगतान बाहरी
साधनों को नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार उत्पादक के स्वयं स्वामित्व वाले साधनों
की लागते सन्निहित (अथवा अस्पष्ट) लागतें हैं। सामान्य लाभ (Normal Profit)
उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है,
उसे सामान्य लाभ कहते हैं।
स्थिर या पूरक लागत (Fixed
or Supplementary Cost )- स्थिर व पूरक लागत वह लागत है जिसमें उत्पादन की
मात्रा में परिवर्तन होने दिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह लागत उत्पत्ति के
स्थिर साधनों के प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है। यह लागत केवल अल्पकाल में उत्पन
होती है। दीर्घकाल में कोई स्थिर लागत नहीं होती है। .
परिवर्तशील लागत (Variable
Cost.) - परिवर्तशील लागत वह लागत है जो उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन होने पर
परिवर्तित होती रहती है। यह लागत उत्पत्ति के परिवर्तनशील लागत के प्रयोग के कारण
उत्पन्न होती है। • कुल लागत (Total Cost) - किसी
वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को जितने कुल व्यय
करने पड़ते हैं। उनके जोड़ को कुल लागत कहते हैं। अल्पकाल की कुल
लागत में स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत दोनों सम्मिलित होती है, जबकि दीर्घकाल
की कुल लागत में केवल परिवर्तनशील लागते ही शामिल होती हैं।
औसत लागत (Average Cost)- उत्पादन की प्रति
इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। औसत लागत (AC) = कुल लागत (TC) उत्पादन मात्रा
(q)
• सीमान्त लागत (Marginal Cost)- किसी वस्तु की एक कम या एक अधिक इकाई का
उत्पादन करने से कुल लागत में जो अन्तर आत है, उसे सीमान्त लागत कहते हैं अर्थात् अतिरिक्त
इकाई की अतिरिक्त लागत को सीमान्त लागत कहते हैं।
• औसत लागत एवं सीमान्त लागत में सम्बन्ध
(Relation between AC and MC) औसत लागत एवं सीमान्त लागत दोनों की गणना कुल लागत
से होती है किन्तु,
(1) जब औसत लागत (AC) गिरती है, तब AC > MO
(2) जब औसत लागत (AC) न्यूनतम होती है, तब AC = MC
(3) यदि औसत लागत (AC) बढ़ती है, तब AC < MC
अल्पकालीन व दीर्घकालीन
लागतें (Short Period and Long Period Costs)- अल्पकाल में कुल लागत (TC) में दो लागतें'
तथा TVC सम्मिलित रहती हैं, परन्तु दीर्घकाल में स्थिर व परिवर्तनशील लागतों के
बीच अन्तर समाप्त हो जाता है क्योंकि दीर्घकाल में साधन परिवर्तनशील होते हैं और
इसलिए सभी लागतें भी परिवर्तनशील होती हैं।
अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन
दोनों AC वक्र U आकार के होते हैं (Both Short Period and Long Period AC Curves Shaped) - अल्पकालीन औसत लागत वक्र तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दोनों ही ए आकृति के
होते हैं, किन्तु दीर्घकालीन लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र की तुलना में
अधिक चपटा (Flatter) होता है। साथ ही दोनों के आकार का होने के
अलग-अलग
हैं। अल्पकालीन औसत लागत के आकार होने का कारण है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम,
जबकि दीर्घकाली लागत के आकार होने का कारण है पैमाने का प्रतिफल ।
उत्पादक या
फर्म का सन्तुलन (Producer's or Firm's Equilibrium)- उत्पादक की सन्तुलन की अवस्था उस समय होती
है जबकि उसके लाभ अधिकतम होते हैं। अधिकतम लाभ के लिए फर्म के कुल आगम (TR) तथा कुल
लागत (TC) का अन्तर अधिकतम हो।
लाभ क्या है? (What is Profit ?) - कुल आगम व कुल लागत के अन्तर
को लाभ कहते हैं (लाभ = कुल आगम- कुल लागत लागत
में सामान्य लाभ सम्मिलित रहता है।
लाभ अधिकतम करने की शर्तें (Conditions of Profit Maximisation)
(1) अनिवार्य शर्त
(Necessary Condition)-सीमान्त लागत (MC) = सीमान्त आगम (MR)
(2) पूरक शर्त
(Supplementary Condition)-सन्तुलन के बिन्दु (अर्थात् जहाँ MR और MC बराबर हैं) पर
सीमान्त लागत रेखा (MC) सीमान्त आगम रेखा (MR) को नीचे से काटे अर्थात् MR और MC की
समानता के बिन्दु पर MC बढ़ती हुई होनी चाहिए। समविच्छेद बिन्दु (Break Even
Point) - यह उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब
TR = TC अथवा MR = MC
पूर्ति (Supply) – वस्तु की वह
मात्रा जो बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत
की जाती है।
स्टॉक (Stock) - यह
वस्तु की वह मात्रा है जो उत्पादकों के पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची (Individual Supply Schedule)-
यह एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की कीमत तथा बेची जाने वाली मात्रा के सम्बन्ध को
प्रकट करती है।
बाजार पूर्ति अनुसूची
(Market Supply Schedule) - यह किसी बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा एक
निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली कुल मात्रा के योग को प्रकट
करती है।
व्यक्तिगत पूर्ति वक्र
(Individual Supply Curve ) - व्यक्तिगत पूर्ति वक्र वह है कि जो विभिन्न
कीमतों पर फर्म द्वारा की गई पूर्ति को प्रकट करती है।
बाजार पूर्ति वक्र (Market
Supply Curve) - बाजार पूर्ति वक्र वह वक्र है जो विभिन्न कीमतों पर बाजार की सभी फर्मों
द्वारा की गई कुल पूर्ति को प्रकट करती है।
सुरक्षित कीमत (Reserved
Price) - जिस कीमत से नीची कीमत पर विक्रेता वस्तु की पूर्ति के लिए तत्पर नहीं
होते, उसे सुरक्षित कीमत कहा जाता है।
पूर्ति फलन (Supply
Function ) - वस्तु की पूर्ति एवं इसके निर्धारक तत्वों के बीच कार्यात्मक सम्बन्ध
(Functional Relationship) को पूर्ति फलन कहा जाता है।
S, = f (P,, P,, P,, T, N, G, E, Gp)
जहाँ, S = वस्तु की पूर्ति,
P1 = वस्तु की कीमत,
P, = सम्बन्धित वस्तुओं की कीमत, तकनीक,
T =
P; = उत्पादन साधनों की कीमत,
N = फर्मों की संख्या,
G = फर्म का उद्देश्य,
G_ = सरकारी नीति ।
E = भविष्य में सम्भावित कीमत,
पूर्ति को प्रभावित करने
वाले तत्व (Factors affecting the Supply of a Commodity)—
(1) वस्तु की कीमत,
(2) स्थानापन्न वस्तु की कीमत,
(3) उत्पादन के साधनों की कीमतें.
(4) तकनीकी स्तर,
(5) बाजार में फर्मों की संख्या,
(6) फर्म का उद्देश्य,
(7) भविष्य में सम्भावित कीमत,
(8) सरकारी नीति ।
• पूर्ति का नियम (Law of Supply) - अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत
बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है।
पूर्ति में परिवर्तन
(Change in Supply) - पूर्ति में परिवर्तन दो रूपों और दो कारणों से
होता है- (1) कीमत परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र पर संचलन। (2) कीमत के अतिरिक्त
अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र का खिसकाव ।
• पूर्ति वक्र पर संचलन (Movement along a Supply
Curve) - केवल कीमत में
परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र पर दो प्रकार का संचलन होता है- (A) पूर्ति का विस्तार,
(B) पूर्ति का संकुचन।
(A) पूर्ति का विस्तार (Extension of Supply)- 'अन्य बातें समान' रहने पर जब किसी वस्तु
की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति अधिक हो जाती है तो इस बढ़ी हुई पूर्ति को पूर्ति
का विस्तार कहा जाता है।
• पूर्ति की लोच (Elasticity of Supply) एक वस्तु
की पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तनों को वस्तु की कीमत के प्रतिश
परिवर्तन में विभाजित करने पर पूर्ति की लोच ज्ञात की जा सकती है। इसको सूत्र रूप में
निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है-
पूर्ति में आनुपातिक या
प्रतिशत परिवर्तन = कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन
QP ΔΟ P Q P अथवा X ΔΡ
Q
• लोचदार पूर्ति की श्रेणियाँ (Degrees of Elasticity of
Supply)—
(1) पूर्णतया लोचदार पूर्ति (Perfectly Elastic
Supply) - जब कीमत में
थोड़ा परिवर्तन होने पर पूर्ति भी शून्य हो जाती है, तब वस्तु को पूर्ति पूर्णतया लोचदार
कही जाती है। (e, = ००)
(2) इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति (Greater than
Unitary Elastic Supply)- जब किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है
तो इस दशा में पूर्ति लोच इकाई से अधिक होती है। (e> 1)
(3) इकाई लोचदार पूर्ति (Unitary Elastic
Supply)- जब किसी वस्तु
की पूर्ति में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन
हुआ है तो उस वस्तु की पूर्ति को इकाई लोच कहते हैं। e = 1)
(4) पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति (Perfectly Inelastic Supply)
- जब कीमत में काफी परिवर्तन आने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन न आये तो पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार कहलाती है। (eg =
0)
पूर्ति की लोच की माप (Measurement of Supply Elasticity)—
AQ/Q AP/P =
(5) इकाई से कम लोचदार पूर्ति (Less than Unitary
Elastic Supply)- जब किसी
वस्तु की पूर्ति में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन
से कम होता है तो इसे पूर्ति की इकाई से कम लोच कहते हैं। (e, < 1)
पूर्ति लोच को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors Influencing
the Elasticity of Supply)— (६) वस्तु की प्रकृति, (ii) उत्पादन लागत, (iii) भावी कीमतों में परिवर्तन की
आशा, (iv) प्राकृतिक अवरोध , (v) उत्पादन तकनीक, (vi) समय तत्व।
पूर्ति की
लोच
पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन/
आरिम्भक पूर्ति मात्रा//